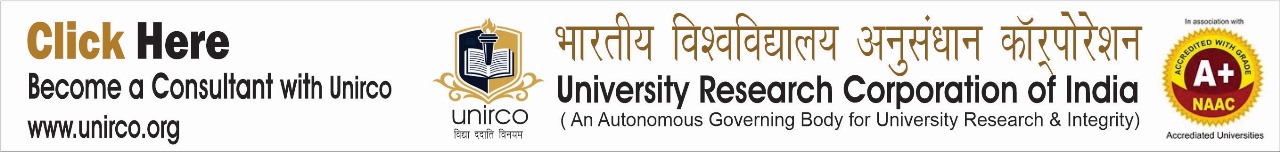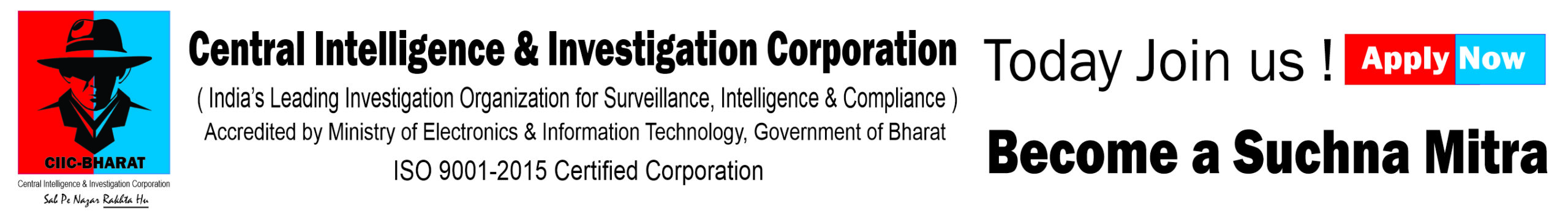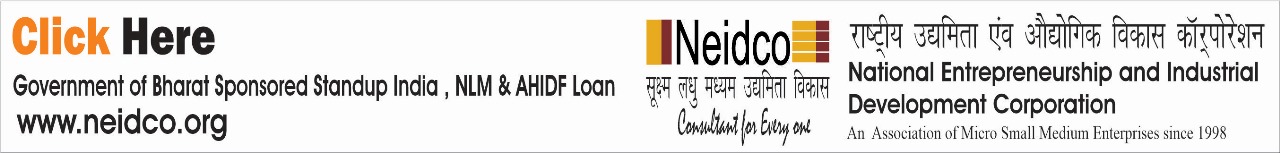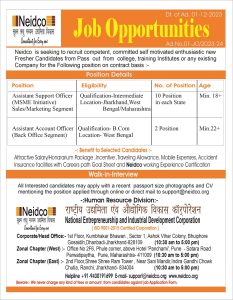
रायपुर-छत्तीसगढ़:-विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए।इसका मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नें अवलोकन किया।मुख्यमंत्री साय नें दो हितग्राही दीपक वाधवानी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आठ लाख रूपए और शबनूर बानों को पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत बीच हजार रूपए का चेक प्रदान किया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 176 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया गया, साथ ही मुख्यमंत्री नें आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया।मुख्यमंत्री नें उज्जवला योजना के तहत इन्द्राणी चन्द्रकार और उषा बाई को नवीन गैस कनेक्शन प्रदान किए।

मुख्यमंत्री साय नें इसके बाद महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल भी पहुंचे और महिला समूहों द्वारा बनाए गए मिलेट्स के उत्पाद की जानकारी ली, साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर आधारित केक काटकर खुशी जाहिर की।मुख्यमंत्री नें विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली।इस अवसर पर आधार सेवा केन्द्र द्वारा 33 नागरिकों के आधार कार्ड अपडेट किए गए।