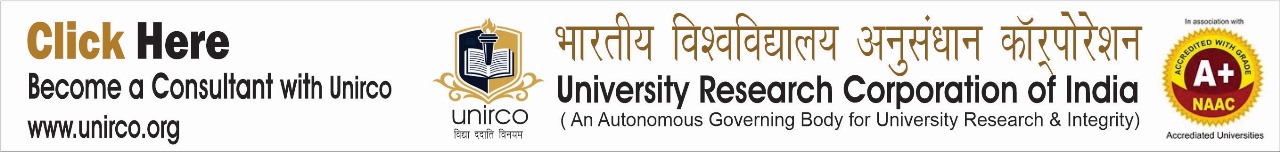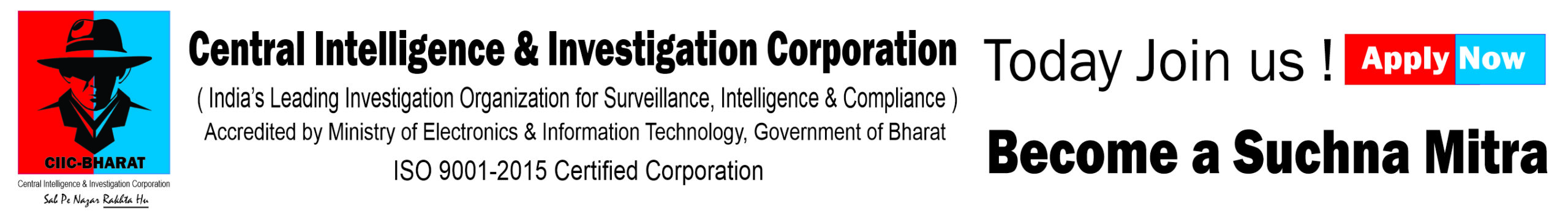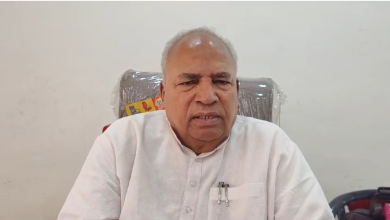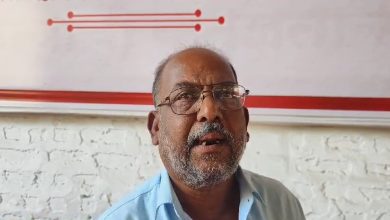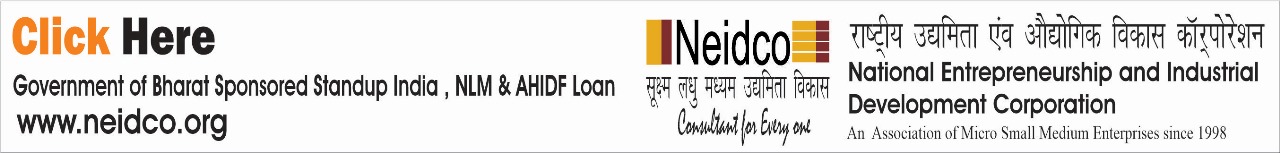नई दिल्ली। बुंदेलखंड की धूल भरी पगडंडियों से लेकर संसद के गलियारों तक पहुँची फूलन देवी भारतीय लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट और विवादास्पद हस्तियों में गिनी जाती हैं। डकैतों के गिरोहों, जातिगत हिंसा और सामाजिक अपमान की वर्षों तक झेली यातना के बाद राजनीति में प्रवेश करने वाली फूलन का अस्तित्व अपने आप में प्रतिरोध, पुनर्निर्माण और दूसरी ज़िंदगी की कहानी है। वर्ष 2000 के इस मोड़ पर, जब राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिक न्याय, महिला आरक्षण और हाशिये के समुदायों की आवाज़ बहस के केंद्र में हैं, फूलन देवी का नाम बार-बार सामने आता है—कभी उम्मीद की तरह, कभी असहमति की तरह, और कई बार एक चुनौती की तरह कि क्या लोकतंत्र सचमुच अपने सबसे वंचितों को प्रतिनिधित्व देता है।
संसद की बेंचों पर बुंदेलखंड की आवाज़
साल 2000 में फूलन देवी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हुई दिल्ली में हैं। गंगा के किनारे बसे इस इलाके की सामाजिक-सांस्कृतिक तस्वीर में खेतिहर मज़दूर, छोटे किसान, कोयला खदानों का श्रम, और बनारसी पट्टी का औद्योगिक-व्यावसायिक दबदबा शामिल है। संसद के भीतर फूलन का फोकस लगातार उन मुद्दों पर रहा है जो ग़रीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं—भूमि सुधार, श्रमिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
लोकसभा में उनके भाषणों का अंदाज़ अकादमिक कम और ज़मीनी ज़्यादा रहता है। अक्सर वे आँकड़ों की जगह सच्ची घटनाओं का हवाला देती हैं—किसान की फसल बिकने के पहले ही गिरवी रखने की मजबूरी, खदानों में सुरक्षा उपकरणों की कमी, या फिर आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों के अभाव का दर्द। विरोधी दल उन्हें ‘भावुक’ कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके समर्थक इसी बेबाक़पन को उनकी ताक़त मानते हैं। मिर्ज़ापुर व आसपास के इलाकों में हुए जन-सुनवाई कार्यक्रमों में उन्होंने छोटी-छोटी शिकायतों—जैसे विधवा पेंशन, राशन कार्ड, या बलात्कार के मामलों में थानों की उदासीनता—को संसद तक पहुँचाने की ज़िद दिखाई है।

महिला आरक्षण बिल और ‘दोगुना आरक्षण’ की माँग
साल 2000 का संसद सत्र महिला आरक्षण के सवाल पर भी तप रहा है। फूलन देवी खुले तौर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करती हैं, पर साथ ही उनके लिए यह आरक्षण ‘समान’ से अधिक ‘समान रूप से सुलभ’ होना चाहिए—यानी अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्पष्ट उप-आरक्षण। उनके मुताबिक़, “बिना उप-आरक्षण के महिला आरक्षण का बड़ा हिस्सा वैसे ही शक्तिसंपन्न घरानों में सिमट जाएगा,”—यह तर्क वे लोकसभा के भीतर और बाहर, दोनों जगह दोहराती हैं। उनके भाषणों में ‘प्रतिनिधित्व’ कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल है; वे कहती हैं कि निर्णय लेने वाली मेज़ों पर वही लोग बैठें जो सामान्य दिनों में दाल-रोटी की जद्दोजहद और असुरक्षा का अनुभव करते हैं।
सुरक्षा का सवाल और राजनीतिक जीवन की कठिन राह
फूलन देवी की सार्वजनिक छवि जितनी तेज़-तर्रार है, उनके राजनीतिक जीवन पर ख़तरे का साया उतना ही घना है। साल 2000 में भी उनके घर और दफ़्तर की सुरक्षा व्यवस्थाएँ चर्चा में रहती हैं। कुछ विरोधी नेता इसे ‘अनावश्यक तामझाम’ कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक इसे उनकी जीवन-यात्रा के जोखिमों और पुराने वैमनस्य की स्वाभाविक परिणति बताते हैं। दिल्ली के सरकारी क्वार्टर से निकलते हुए उनकी सुरक्षा टुकड़ी का काफ़िला आम दृश्य बन चुका है—यह दृश्य जितना असहज करता है, उतना ही एक वास्तविकता भी बताता है कि अतीत के घाव ज़िद्दी होते हैं।
‘बैंडिट क्वीन’ से परे: एक निजी जीवन, सार्वजनिक बहस
फूलन देवी पर बनी फ़िल्म बैंडिट क्वीन ने 90 के दशक में उनकी छवि को दुनिया भर में चर्चित किया था। फ़िल्म का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि बहुतों के लिए फूलन की कहानी वही बने दृश्य बन गई। मगर वर्ष 2000 में, वे लगातार यह रेखांकित करती दिखती हैं कि फ़िल्म एक रचनात्मक प्रस्तुति है—उसके बाहर भी उनकी ज़िंदगी है: एक सांसद, एक पत्नी, एक नागरिक और सबसे पहले एक महिला, जो रोज़ नए मायनों में अपनी पहचान गढ़ रही है। फ़िल्म पर उनकी असहमति और उससे जुड़े कानूनी पेंच ने इसी बात पर रोशनी डाली कि किसी व्यक्ति की निजी पीड़ा और सार्वजनिक विमर्श के बीच एक महीन रेखा होती है—और उसे लाँघना आसान नहीं।
न्याय, क्षमा और स्मृति के बीच
फूलन देवी का नाम आते ही न्याय और प्रतिशोध की बहसें साथ-साथ चल पड़ती हैं। बीते वर्षों में उन पर लगे गंभीर आरोप, अदालतों की प्रक्रियाएँ, और रिहाई से जुड़ी राजनीति—सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। वर्ष 2000 में भी इनके कानूनी पक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, और अक्सर वे विरोधी दलों के लिए राजनीतिक निशाना बन जाते हैं। लेकिन उनके समर्थकों का तर्क है कि राज्य ने जब उन्हें वैधानिक प्रक्रिया से मुक्त जीवन दिया और जनता ने उन्हें संसद पहुँचाया, तो यह दोनों ही घटनाएँ उनके सामाजिक पुनर्वास की मान्यता हैं। सवाल यह नहीं कि अतीत को भुला दिया जाए; सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर पहचाना जाएगा, या हमेशा अतीत की परछाइयों में कैद रखा जाएगा?

मिर्ज़ापुर के वादे और धरातल की हक़ीक़त
साल 2000 में उनके संसदीय क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ गंभीर बनी हुई हैं—टूटी सड़कें, सीमित सिंचाई, और रोज़गार के सीमित अवसर। लोक निर्माण परियोजनाओं के बारे में उनके दफ़्तर से नियमित अपडेट जारी होते हैं—किस सड़क का मरम्मत टेंडर लगा, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ़ की तैनाती हुई, किस रेलवे हॉल्ट के विस्तार पर फाइल आगे बढ़ी। यह सबक कुछ मतदाताओं को ‘धीमी’ रफ़्तार लगता है, क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं और संसाधन सीमित। फिर भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठकों में उनकी मौजूदगी और सीधे फोन उठाकर अफ़सरों से बात करने का अंदाज़—यह भरोसा बनाता है कि ‘काम हो तो सकता है, लड़ाई चाहिए।’
जाति, लिंग और सत्ता: एक असहज संवाद
भारतीय राजनीति में जाति एक यथार्थ है। फूलन देवी इस यथार्थ को छुपाती नहीं, बल्कि खुलकर चर्चा करती हैं। वे बताती हैं कि स्त्री, वह भी दलित/पिछड़े समुदाय की स्त्री, सत्ता के ढाँचों में कितनी बार अदृश्य कर दी जाती है—कभी भाषा के स्तर पर, कभी प्रक्रिया के स्तर पर, और सबसे ज़्यादा संसाधनों की पहुँच के स्तर पर। वे संसद में बार-बार कहती हैं कि पुलिस सुधार और न्यायिक पहुँच को ‘लैंगिक और सामाजिक संवेदनशीलता’ के साथ डिज़ाइन किया जाए—थानों में महिला हेल्प डेस्क, तेज़तर्रार पीड़ित सहायता तंत्र, और गवाह सुरक्षा जैसी चीज़ें सिर्फ़ महानगरों का विशेषाधिकार न रहें।
विपक्ष के सवाल और राजनीतिक जवाब
स्वाभाविक है कि विपक्ष फूलन देवी पर सवाल उठाए—उनके अतीत, अदालतों की कार्यवाहियों, और फ़िल्मी छवि का राजनीतिकरण। कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी लोकप्रियता ‘करुणा’ पर टिकी है, न कि ‘शासन’ पर। इसके जवाब में फूलन का तर्क सीधा है: “शासन वहीं मजबूत होगा जहाँ आख़िरी व्यक्ति दिखाई देगा।” वे यह भी कहती हैं कि गाँवों की गलियों, खदानों के मज़दूरों और रेहड़ी-पटरी की महिलाओं के सवाल तथाकथित ‘बड़े’ मुद्दों से छोटे नहीं हैं। उनके भाषणों में ‘विकास’ का अर्थ सड़कों और पुलों के साथ-साथ सामाजिक सम्मान और सुरक्षा की भावना से भी है—“किसी का सिर झुके नहीं, यह भी विकास है।”
एक ‘प्रतीक’ होने का बोझ
जन-नेताओं के साथ अक्सर यह दिक़्क़त रहती है कि वे ‘प्रतीक’ बन जाते हैं—और प्रतीक बनते ही उनसे असंभव उम्मीदें जोड़ी जाती हैं। फूलन देवी इस बोझ को स्वीकार भी करती हैं और उससे जूझती भी हैं। वे जनता से कहती हैं कि उन्हें देवी मत बनाइए—“मैं आपकी तरह एक आदमी (इंसान) हूँ, ग़लतियाँ मुझसे भी होती हैं।” यह स्वीकारोक्ति उन्हें मानवीय बनाती है; एक ऐसी व्यक्तित्व-छवि, जहाँ त्रुटियाँ हैं, पर उनसे सीख लेने की जिद भी है। आलोचक कहते हैं कि यही ‘मानवीयता’ कभी-कभी प्रशासनिक सख़्ती में कमी की वजह बनती है; समर्थक कहते हैं कि इसी से लोकतंत्र का चेहरा नरम होता है।
मीडिया, मिथक और वास्तविकता
मीडिया में फूलन देवी की कहानी अक्सर ‘दाँव और तलवार’ के रूपकों में सिमट जाती है। लेकिन साल 2000 में, देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ नए गठबंधन, नई सामाजिक समीकरण और आर्थिक उदारीकरण की दूसरी लहर के बीच नायक-नायिका की सटीक परिभाषाएँ ढह रही हैं। ‘बाग़ी’ और ‘नेता’ के बीच की दूरी अब उतनी नहीं रही; समाज अपने प्रतिनिधियों से ‘कहानी’ ही नहीं, ‘काम’ भी माँग रहा है। इसी संदर्भ में फूलन देवी की वास्तविक परीक्षा सिनेमा के पर्दे पर नहीं, बल्कि संसदीय समितियों, बजट आवंटनों और ज़मीनी परियोजनाओं में है—जहाँ वे फ़ाइलों की भाषा सीख रही हैं और उस भाषा में अपने लोगों की बोली मिला रही हैं।
संगठित अपराध, पुलिस सुधार और न्याय प्रक्रिया
फूलन देवी की अपनी जीवन-कथा ने उन्हें अपराध-न्याय तंत्र की कमियों और मजबूरियों दोनों से रूबरू कराया है। संसद में वे गवाह सुरक्षा, तेज़-तर्रार सुनवाई, और पीड़ित सहायता का बार-बार मुद्दा उठाती हैं। उनका तर्क है कि कानून का राज तभी मज़बूत होगा जब ‘डर’ केवल अपराधियों में हो, पीड़ितों में नहीं। वे यह भी सुझाती हैं कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या थानों में बढ़े, और हर ज़िले में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर हों—जहाँ मेडिकल, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहयोग एक छत के नीचे मिले। यह सोच उन्हें ‘कठोर’ और ‘संवेदी’—दोनों बनाए रखती है।
दिल्ली के गलियारे, गाँव की चौपाल
दिल्ली के शीतकालीन सत्र की भागदौड़ के बीच जब फूलन अपने क्षेत्र लौटती हैं, तो चौपालों पर बैठकों का सिलसिला देर रात तक चलता है। ग्रामीण महिलाएँ अक्सर अपने सिर पर आँचल खींचे, धीरे-धीरे बोलती हैं; फूलन उनसे कहती हैं—“ऊँची आवाज़ में बोलो, डरना नहीं।” यह दृश्य किसी राजनीतिक रैली की नहीं, बल्कि भरोसा जगाने की कसरत का है। वे मध्यस्थ का रोल भी निभाती हैं—जहाँ प्रधान और सचिव के बीच अनापत्ति प्रमाण पत्र पर अटकाव हो, या मनरेगा जैसे योजनागत भुगतान (तब के संदर्भ में ग्रामीण रोज़गार योजनाएँ) में देरी हो, वहाँ वे सीधे ज़िला प्रशासन से हस्तक्षेप कराती हैं।
विकास का वैकल्पिक खाका
फूलन देवी ‘हाईवे’ के साथ-साथ ‘घरेलू आँगन’ के विकास की बात करती हैं—यानी पेयजल, शौचालय, स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति, और प्रसव पूर्व-पश्चात देखभाल। वे ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और माइक्रो-क्रेडिट मॉडल को मिर्ज़ापुर के पहाड़ी-पठारी इलाकों के हिसाब से ढालने की बात करती हैं—जहाँ छोटी पूँजी से कुटीर उद्योग, बकरी पालन, या टेराकोटा/हस्तशिल्प जैसे कामों को बढ़ावा मिल सके। उनके दफ़्तर ने कुछ जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण शिविर कराए हैं—सिलाई, अगरबत्ती, और पत्तल बनाने जैसे कामों में। इन पहलों का असर धीमा लेकिन स्थिर बताया जाता है—क्योंकि यह ‘काम देकर सम्मान’ का रास्ता खोलता है।
राजनीतिक समीकरण और भविष्य की राह
वर्ष 2000 में राष्ट्रीय राजनीति गठबंधन युग से गुजर रही है। बड़े राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय और सामाजिक न्याय की राजनीति ने अपनी साख बनाई है। फूलन देवी इसी बड़े कैनवस पर एक छोटे लेकिन चमकीले ब्रश-स्ट्रोक की तरह नज़र आती हैं—वे संख्या नहीं, प्रतीक की राजनीति करती हैं; पर यह प्रतीकवाद रिक्त नहीं है, इसके पीछे अपनी सामाजिक जड़ों का नेटवर्क और मतदाताओं की उम्मीदें हैं। प्रश्न यह है कि क्या वे आने वाले वर्षों में इस प्रतीकवाद को संस्थागत उपलब्धियों—क़ानूनों, योजनाओं और बजट—में तब्दील कर पाएँगी? आलोचक कहते हैं कि प्रशासकीय दक्षता और टीम-निर्माण उनकी अगली परीक्षा हैं; समर्थक मानते हैं कि सीखने की उनकी गति तेज़ है और मंतव्य साफ़—‘सबका सम्मान, बराबरी के साथ।’
‘दूसरा मौका’ और लोकतंत्र का वादा
फूलन देवी की कहानी दरअसल ‘दूसरा मौका’ देने की सामाजिक और संवैधानिक क्षमता की कसौटी है। क्या हमारा समाज किसी स्त्री को, जो अंधेरों से निकलकर आई है, नया परिचय दे सकता है? क्या हमारा राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्याय न तो बदले की भाषा बोले और न ही उदासीनता की? वर्ष 2000 में, जब देश नई सदी में अपने कदम टटोल रहा है, फूलन देवी एक याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र केवल वोट का गणित नहीं—यह स्मृति, करुणा, न्याय और सुधार की लंबी यात्रा भी है।
बहस जारी रहे—यही ज़रूरी है
साल 2000 की राजनीति में फूलन देवी का स्थान उस बहस का केंद्र है जो कहती है—‘कौन बोलेगा, किसके लिए बोलेगा, और क्या बोला जाएगा।’ उनकी उपस्थिति से सत्ता के गलियारों में असहज सवाल उठते हैं, और यह असहजता ही लोकतंत्र को जाग्रत रखती है। वे अपने अतीत से आँख मिलाकर चलती हैं, वर्तमान में अपने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ती हैं, और भविष्य के लिए ऐसे भारत का ख्वाब देखती हैं जहाँ लड़कियाँ बिना डर स्कूल जाएँ, जहाँ खेतिहर मज़दूर का पसीना इज़्ज़त में बदले, और जहाँ संसद की कुर्सियाँ उन लोगों से भरी हों जिनकी आवाज़ आज भी कई बार दबा दी जाती है।
फूलन देवी का यह सफ़र अभी मुकम्मल नहीं—यह एक जारी संवाद है। और संभवतः, एक लोकतांत्रिक देश के लिए इससे बड़ी ख़ुशक़िस्मती क्या कि उसके भीतर ऐसे संवाद बने रहें, चलते रहें, और दिशा दिखाते रहें